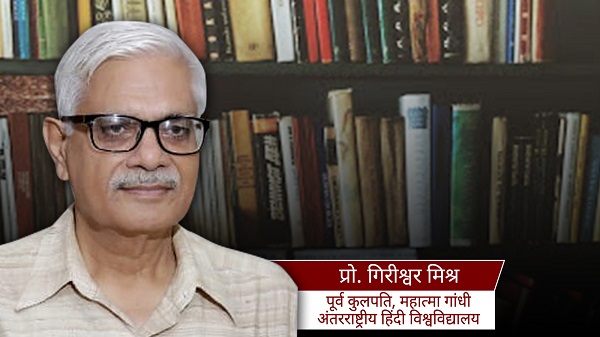Professor Durganand Sinha: संस्कृति-संवाद के आग्रही मनोविज्ञानी प्रोफ़ेसर दुर्गानन्द सिन्हा (1922-1997)
Professor Durganand Sinha: मनुष्य होना एक सांस्कृतिक उपलब्धि है और संस्कृति में रह कर सृजनात्मक संवाद करते हुए ही मनुष्यों के बारे में प्रामाणिक और उपयोगी ज्ञान पाया जा सकता है। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय मूल का स्वदेशी मनोविज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि इस क्षेत्र का इतिहास। जिन वेदों और उपनिषदों से मन और चेतना के कई सिद्धांत निकले हैं, वे कम से कम तीन हज़ार साल पुराने हैं। भावना, संज्ञान तथा सामाजिक आचरण आदि को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार-मंथन हुआ है। यह बौद्धिक परंपरा इस अर्थ में बहुलतावादी है कि इसने सांख्य, वेदांत, न्याय, मीमांसा आदि के साथ चार्वाक, बौद्ध और जैन सहित अलग-अलग विचार धाराओं का आदर किया और उनके सह अस्तित्व को स्वाभाविक मानते हुए वैचारिक विमर्श में शामिल किया।
विविध विचार-प्रणालियाँ, जो अलग-अलग राह पर चलने वाली हैं, यहाँ तक कि जो परस्परविरोधी भी लगती हैं उन्हें भी विचार में पूरी प्रामाणिकता के साथ जगह दी । परंतु जब एक आधुनिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान विषय का शिक्षण औपनिवेशिक शासन के दौर में 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तो वह यहाँ के परम्परागत ज्ञान से विलग एक शुद्ध आयातित विषय के रूप में शामिल किया गया । अंग्रेजों की शैक्षिक नीति ने ज्ञान और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की भारतीय परंपराओं को अकादमिक जगत की मुख्यधारा से व्यवस्थित रूप से हाशिए पर डाल दिया। परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक विज्ञान के यूरो-अमेरिकी संस्करण का ही प्रचार-प्रसार हुआ और भारतीय विचार-प्रणालियों में उपलब्ध मनोवैज्ञानिक घटनाओं, प्रवृत्तियों और गोचरों के बारे में समृद्ध और विविधतापूर्ण विचार-विमर्श बहिष्कृत ही रहा।
काफ़ी दिनों तक मनोवैज्ञानिक विषयक ज्ञान की ये दो परंपराएँ अलग-थलग पड़ी रहीं और गैर-संदर्भित मनोविज्ञान की एक अकादमिक परियोजना पुष्पित-पल्लवित होती रही। वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता के आग्रह और पश्चिम से स्वीकृति पाने के आकर्षण में पश्चिमी दृष्टिकोण को मानक की जगह दी गयी। उसे ही ज्ञान का मानते हुए अध्ययन-अध्यापन और शोध की दिशा निर्धारित हुई। ऐसे में भारतीय समाज पश्चिमी सिद्धांतों और स्थापनाओं की जाँच की प्रयोगशाला बन गया। इस तरह के उधार वाले विषय की सांस्कृतिक प्रासंगिकता की कमी ने समस्या-समाधान और सैद्धांतिक नवाचार के लिए अन्य विषयों की तरह भारतीय मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और उपयोग की क्षमता को काफी सीमित कर दिया।
वैश्वीकरण की प्रवृत्तियाँ, बढते हुए अंतरसांस्कृतिक संचार, और सांस्कृतिक विविधता की स्वीकृति ने सांस्कृतिक संवेदना से समृद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ जुड़ने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया है। इस दृष्टि से स्वदेशीकरण के आंदोलन ने कई रूप लिए हैं और विभिन्न देशों में मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिकगर्भित मनोविज्ञान के निर्माण में संलग्न हैं। इस आंदोलन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के पहले प्रोफेसर दुर्गानन्द सिन्हा ने अग्रणी भूमिका निभाई। पटना में दर्शन के अध्ययन के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कार्य मनोवैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृति की सत्ता का सम्मान करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और बताते हैं कि विषय को समाज के लिए किस तरह प्रासंगिक बनाया जा सकता है और मनोवैज्ञानिक ज्ञान-सृजन को पश्चिम के अनुकरण की जगह सृजनात्मक कैसे बनाया जा सकता है। ज्ञान के इकतरफ़ा प्रवाह की जगह पारस्परिक संवाद को उन्होंने महत्व दिया। सन1965 में एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में उनका लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें भारतीय मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के रिश्तों की गहन पड़ताल की गयी थी।
बढ़ती हुई बेचैनी ने इस विषय के पुनर्विन्यास की दिशा में सोचने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। राजनीतिक स्वराज के साथ वैचारिक स्वराज की स्थापना भी आवश्यक मानी गयी। इस दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने कई युक्तियों या रणनीतियों का सहारा लेना आरम्भ किया और सांस्कृतिक संदर्भ के साथ-साथ विविध मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार संबंधी घटनाओं के बारे में स्वदेशी ज्ञान-प्रणालियों का सम्मान करने के लिए कई मार्गों को अपनाना आरम्भ किया ।इस तरह के प्रयास चेतना, योग, आत्म, स्वास्थ्य, स्वस्ति भाव, नेतृत्व और कल्याण सहित कई क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं। यह तेजी से महसूस किया जा रहा है कि प्रामाणिक समझ, अनुप्रयोग और अपेक्षित बदलाव लाने की दृष्टि से मनोविज्ञान की क्षमता को बढ़ाने के लिए संस्कृति को सिद्धांत के साथ-साथ अध्ययन की कार्यप्रणाली अर्थात् विधियों में एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
यद्यपि मुझे प्रोफ़ेसर सिन्हा के विद्यार्थी होने का अवसर नहीं मिला था परंतु वर्ष 1974 में सम्पर्क में आने के बाद जो स्नेह सम्बन्ध बना वह मेरे दृष्टिकोण, अनुसंधान , लेखन और व्यावसायिककार्यकलापों के लिए निर्णायक कारक साबित हुआ। मैंने 1978 से1983 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके सहयोगी के रूप में अध्यापन किया । इस दौरान उनके साथ मिल कर शोध, लेखन और चर्चा का जो क्रम शुरू हुआ वह अगले दो दशकों में प्रगाढ़ होता गया । अगले दस वर्ष मैं भोपाल में रहा और प्रोफ़ेसर सिन्हा का प्रेरक सान्निध्य लगातार मिलता रहा ।
इसी दौरान भारत में अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान विषय पर महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई जिसमें प्रोफ़ेसर सिन्हा और अन्य मनोवैज्ञानिकों के साथ गहन संवाद हुआ। यहीं पर मनोविज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी के गठन के विचार को मूर्त रूप देने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब मैं 1993 में दिल्ली आया तो संस्कृति और मनोविज्ञान विषय पर बहु अनुशासनात्मक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें प्रो सिन्हा की प्रमुख भागीदारी थी। वे यहाँ अतिथि प्राध्यापक के रूप में भी रहे। उनकी संक्रामक उपस्थिति और भागीदारी ने भारत के मनोविज्ञान जगत को सांस्कृतिक परम्परा की प्रासंगिकता से जोड़ने का काम किया।
प्रोफ़ेसर सिन्हा (Professor Durganand Sinha) की रुचि गावों की उन्नति के मनोसामाजिक घटकों को समझने में थी। इस उत्सुकता को लेकर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास के अध्ययन का केंद्र स्थापित स्थापित किया। सामाजिक विकास, ग्रामीणों की प्रेरणा आदि को देखना-समझना आसान न था । वर्ष 1969 में प्रकाशित इंडियन विलेजेज इन ट्रांज़िशन अपने ढंग का पहला मनोवैज्ञानिक प्रयास था। इस अध्ययन ने मनोविज्ञान को एक नए धरातल पर स्थापित करने की चुनौती थी। गाँव के समाज में हो रहे बदलाव, वहाँ पर नेतृत्व, ग्रामीण जनों की जीवन-दृष्टि , उनकी आशाएँ और आकांक्षाएँ आदि को समझने के क्रम में प्रोफ़ेसर सिन्हा ने समष्टि या ‘मैक्रो’ स्तर पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन की चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकृत पैराडाइम को प्रश्नांकित किया । इसी तरह उन्होंने इंद्रियानुभविक अध्ययन के तौर-तरीक़ों को संस्कृति के अनुरूप ढाला न कि पाश्चात्य शोध-उपकरणों को ज्यों का त्यों स्वीकार किया ।
उन्होंने पीढ़ियों के बीच के अंतर को मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख कर समझने का प्रयास किया । यह जानने का भी प्रयास किया कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत क्या हैं ? सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश के प्रति संवेदना का ही परिणाम था कि नैतिक मूल्यों का विकास, बच्चों के पालन-पोषण की पद्धति, परिवार की संरचना में परिवर्तन, परिवार का स्वरूप, और परिवार की पारिस्थितिकी जैसे विषयों को लेकर भारत में इनके अध्ययन की नई ज़मीन तैयार की।
भारत में आत्मबोध का स्वरूप क्या है इस जिज्ञासा को वैयक्तिकतावाद और सामूहिकता की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के विमर्श में देखने का उनका प्रयास नई सैद्धांतिक और इंद्रियानुभविक पहल थी। किस तरह भारतीय परिवेश में समाजीकरण होता है और समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आए हैं इसे जानने की पहल की । उन्होंने अनेक सामाजिक मुद्दों को लेकर अध्ययन आरम्भ किए । इस दृष्टि से उनके कुछ प्रमुख शोध विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, चिंता, उद्योग, प्रवाद, पर्यावरण, ग़रीबी और वंचन, मूल्यों की संस्कृति, स्मृति, तथा प्रत्यक्षीकरण के विकास पर केंद्रित थे।
प्रो सिन्हा के अध्ययनों में संस्कृति सदैव केंद्र में बनी रही और शोध समस्या और उसके अध्ययन की प्रविधि उसी के अनुकूल रहती थी। धीरे-धीरे प्रोफ़ेसर सिन्हा संस्कृति के साथ मनोविज्ञान के सम्बन्धों के सिद्धांतकार की भूमिका में आ गए। वे अंतरराष्ट्रीय अंत: सांस्कृतिक मनोविज्ञान परिषद की स्थापना से जुड़े और बाद में उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारतीय होने का अर्थ और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण, भारत में मनोविज्ञान विशेषतया समाज मनोविज्ञान का विकास, देशीकरण की प्रक्रिया, एशिया का मनोविज्ञान, ग़ैर-पश्चिमी मनोविज्ञान-दृष्टि, अंत: सांस्कृतिक अध्ययन, संस्कृति की दृष्टि से उपयुक्त मनोविज्ञान और संस्कृति का मनोवैज्ञानिक शोध में उपयोग आदि पर शोध और प्रकाशन किया जिसने देश विदेश में अध्येताओं का ध्यान खींचा। संगठनों का सांस्कृतिक आयाम भी उनकी चिंता में बना हुआ था । स्व या आत्म की भारतीय दृष्टि को विकसित करने वाला व्यक्ति वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या पर भी विचार करता था।
स्वस्ति भाव या कल्याण का उनका विचार परिस्थितियों को स्वीकार कर प्रतिकार की क्षमता को भी स्थान देता है। उनके विचार में अध्ययन विधि किसी अध्ययन की सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि विधि लक्ष्य नहीं बल्कि उपकरण होती है। वे विषय के विवेचन में पूर्वापर का सदैव ध्यान रखते थे और विषय प्रतिपादन में ऐतिहासिक दृष्टि को बनाए रखते थे । उन्होंने उत्साह और अकादमिक सक्रियता के साथ संस्कृति से संवाद कैसे स्थापित हो इस पर निरंतर गहन विचार किया और उसे लक्ष्य और संसाधन दोनों ही रूपों में देखा और उसकी शक्ति को पहचाना।
प्रो सिन्हा संस्था का निर्माण करने के साथ विषय को सतर्क और प्रभावी अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया । उनकी वैचारिक उदारता अनुकरणीय थी । संवाद की उत्सुकता , अनुभव को साझा करने की तत्परता लिए देश-विदेश में नए स्थानों को देखने जानने के लिए तैयार प्रो सिन्हा के पास विभिन्न संस्कृतियों की कथाओं का जीवंत ख़ज़ाना था जिसे अनौपचारिक बात चीत में वह अक्सर साझा करते थे । चीन , ब्रिटेन , जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ़्रीका सब जगह उनके मित्र थे और उन्होंने यात्राएँ की थीं । भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वे जाते रहते थे । अकादमिक उद्यमिता की प्रतिमूर्ति बने प्रोफ़ेसर सिन्हा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अकादमिक साझेदारी और सहयोग के अप्रतिम उदाहरण थे । उनके अध्यापन में पुस्तकीय प्रतिपादन की जगह जीवन के अनुभव से लिए उदाहरण महत्वपूर्ण होते थे जो सिद्धांतों के उपयोग को समझने में सहायक होते थे और प्रस्तुति को अनावश्यक नीरसता से बचाते थे ।
जीवन को समग्रता में ग्रहण करते हुए वे हास्य व्यंग के साथ अपने निकट के परिवेश को सदैव जीवंत बनाए रखते थे । अध्ययन-अनुसंधान और लेखन में वे गम्भीर रहते थे और संगोष्ठियों में पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुति करते थे । उनकी पसंद नापसंद भी स्पष्ट रहती थी । उन्होंने मनोविज्ञान विषय के परिसर का विस्तार किया और अन्य परम्पराओं के साथ सम्पर्क साधा । इतनी विविधता वाली संलग्नता किसी के लिए भी स्पृहणीय हो सकती है । उन्होंने संस्था का निर्माण किया और एक श्रेष्ठ सहयोगियों का दल गठित किया और एक उच्च अध्ययन केंद्र स्थापित किया जहां अंतरराष्ट्रीय विचार विनिमय की परम्परा स्थापित की । विषय की उन्नति के लिए उनके निजी और संस्थागत प्रयासों को प्रतिष्ठा भी मिली । उन्होंने मनोविज्ञान के सोच-विचार के मुहावरों को बदला और आरोपित ढाँचे की सतत समालोचना भी की ताकि नवोन्मेषी दृष्टि का विकास हो ।
आज जब वैश्वीकरण, बहुलतावाद और मनोविज्ञान के अनुशासन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चर्चा हो रही है तो स्वदेशीकरण की यात्रा में आने वाली दुविधाओं और चुनौतियों पर भी विचार आवश्यक है और इस दृष्टि से प्रो सिन्हा के विचार और कार्य प्रासंगिक बने हुए हैं।
यह भी पढ़ें:-Indians donations: भारतीय परिवार यहां करते हैं सबसे ज्यादा दान, अध्ययन में हुआ खुलासा…
देश की आवाज की खबरें फेसबुक पर पाने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें