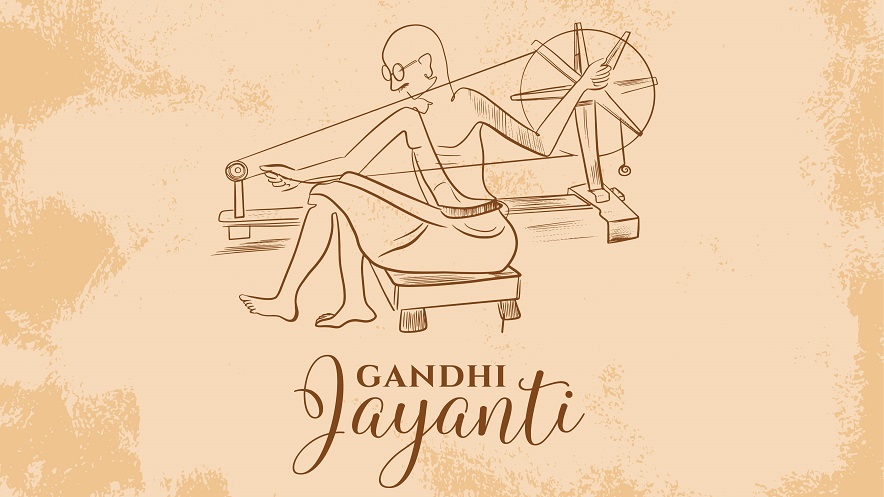Swadeshi: ‘स्वदेशी’ है आत्मबल से उत्कर्ष का आह्वान: गिरीश्वर मिश्र
Swadeshi: बुद्धिमान और सफल होने की चाह रखने वाले के व्यक्ति के लिए महान नीतिज्ञ आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख दी गई है। इसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति को उसका समय कैसा चल रहा है यानी वर्तमान और भविष्य की समझ होनी चाहिए।
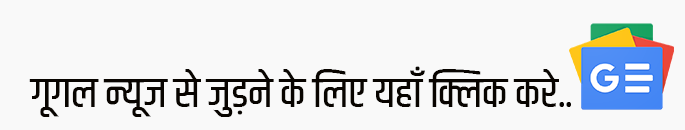
Swadeshi: उसे इस बात का भी ठीक पता होना चाहिए कि मेरे हित-मित्र कौन हैं। उसे अपने परिवेश अर्थात् आस-पास की क्या परिस्थिति है इसका पता होना चाहिए। आमदनी और खर्च कैसे हो रहा है अर्थात् उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। पर इन सबसे ज़्यादा जरूरी है इस बात का आकलन कि मैं कौन हूँ अर्थात् अपने अस्तित्व, अस्मिता और परिस्थिति का वास्तविक आकलन होना चाहिए। साथ ही अपनी क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य का भी पता होना चाहिए।
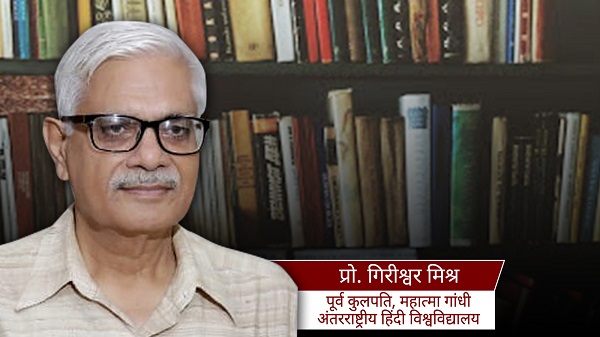
चाणक्य कहते हैं कि इन प्रश्नों पर बार-बार विचार करते रहना चाहिए। तभी व्यक्ति के द्वारा सही निर्णय हो पाता है और जीवन में आने वाली समस्याओं और विघ्न-बाधाओं का निवारण कराटे हुए उनसे पार पाया जा सकता है। यह बात व्यक्ति ही नहीं देश और समाज जैसी इकाई पर भी पूरी तरह लागू होती है। देश को भी अपने देश काल की सीमाओं में रहते हुए सतत आत्मान्वेषण और अपनी शक्ति का संधान करते रहना अपनी पहचान को स्थापित और संवर्धित करने की पहली शर्त हो जाती है ।
आत्मालोचन करने में किसी तरह की ग़फ़लत होने पर मार्ग से भटक जाने की संभावना रहती है, हमारे बने बनाये काम भी बिगड़ सकते हैं और हम लक्ष्य से विचलित भी हो सकते हैं । पर मुश्किल यह है कि यह आत्मान्वेषण कोई स्थायी स्थिति या उपलब्धि नहीं होती कि एक बार तजबीज कर लेने के बाद हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाय और फिर किसी पुनर्विचार या की जरूरत ही न पड़े। इसके लिए व्यक्ति और समाज दोनों को ही अपने आपको निरंतर जाँचते और परखते रहने की जरूरत होती है क्योंकि परिवेश स्वभाव से ही अस्थिर और परिवर्तनशील होता है। इस संदर्भ में देश में स्वदेशी की समकालीन गूंज विशेष महत्व रखती है।
देश का इतिहास गवाह है कि आत्मालोचन की ओर से मुँह मोड़ना आत्मघाती हो जाता है। हमने देखा है कि परतंत्र भारत के राजनैतिक जीवन में बहुत समय तक अपने आत्म-बोध को लेकर ऐसी कई नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हाबी रहीं कि विश्व के प्रथम लोक तंत्र की यह जन्म भूमि पर विदेशी आक्रांताओं के अधीन हो गई और कई शताब्दियों तक उनके ही अधीन रहना पड़ा। उनका आकर्षण स्पष्ट रूप से भारत की समृद्धि के प्रति लोलुप दृष्टि के चलते था। इसलिए विदेशी शासन का उद्देश्य भारत का कल्याण करना नहीं वरन् भारत भूमि पर आधिपत्य जमा कर उसको अपना गुलाम बनाए रखना था । उनकी मुख्य रुचि अपने लिए यहाँ पर उपलब्ध सभी संसाधनों का यथाशक्ति दोहन करने में ही थी।
उन्होंने शोषण और दमन करने के लिए कई अमानवीय तरकीबें भी अपनाईं और भारतीय समाज को तरह-तरह पीड़ित करते रहे। उनके शोषण और दमन के दुश्चक्र ने देश के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय हितों को बड़ी ठेस पहुँचाई। भौतिक, सामाजिक और मानसिक रूप से त्रस्त करते उन्होंने देश को कमजोर किया ताकि उनका अपना उद्देश्य पूरा होता रहे। गौर तलब है कि भारत के साथ इनका कोई विनिमय का रिश्ता नहीं था। यह जरूर हुआ कि कई सदियों तक टिके और पसरे परतंत्रता के इस लंबे दौर में भारत का अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ जो अनिवार्य संपर्क हुआ उसके विविध प्रकार के प्रभाव भी पड़े। उसके फलस्वरूप ख़ान–पान, भाषा-बोली, वेश-भूषा तथा शिक्षा-दीक्षा आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन आए।
इस क्रम में अंग्रेजी शासन के दौरान जो उपनिवेशवादी और तथाकथित आधुनिक दृष्टि का प्रसार हुआ उसने इतिहास, भूगोल ही भारतीय मानस को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त और अस्त-व्यस्त किया। यहाँ पर अपनी संस्कृति-सभ्यता के विभिन्न पक्षों जैसे – कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, आचार-विचार और रहन-सहन को प्रश्नांकित करते हुए झकझोरा और विस्थापित किया । उनकी उपादेयता को लेकर भारतीयों के मन में यथासंभव वितृष्णा जगाई।
यह भी पढ़ें:- New Amrit Bharat Express: प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुर–उधना के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई
भारतीयों के मन में भारत और भारतीयता की पुरातात्विक छवि को बैठाने की भरसक कोशिश की गई और भारतीय ज्ञान-विज्ञान को निरस्त करते हुए पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान की एकल सत्ता स्थापित करने और उसके वर्चस्व को सुदृढ करने की खूब कोशिश हुई। यह तो उसकी जिजीविषा की आंतरिक शक्ति है जिसके चलते उसके मूल स्वर अप्रतिहत बने रह सके ।
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में कई धारायें थीं पर उन सबके मूल में आत्मबोध की ही चिंगारी थी। अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली सारी यातनाओं ने भारतीय समाज के आत्मबोध को आहत किया था । उसी आत्मबोध को लौटाने और पुन:स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी का बिगुल बजाया। उन्होंने अनुभव किया कि आज़ादी का अर्थ स्वराज (सेल्फ रूल) है यानी अपने ऊपर अपना राज। यह सिर्फ़ अपने देश में अपना राज तक ही सीमित नहीं है। इसकी शर्त आत्म-बोध और आत्म-नियंत्रण ही होता है। सहज अर्थ में यह अपने मूल की और लौटने का भी आवाहन है।
गांधी जी देश स्वतंत्रता को राजनैतिक सत्ता-बदल से आगे जाकर वैचारिक और मानसिक स्वाधीनता के अर्थ में ग्रहण करते थे। इसी के लिए वे रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देते थे। अपनी भाषा, अपने उत्पाद, अपने उपकरण, अपनी शिक्षा और अपनी व्यवस्था को स्थानीयता से भी जोड़ कर देखते थे। अस्पृश्यता-निवारण, श्रम पर ज़ोर और मशीनों के सीमित उपयोग के पीछे उनकी यही मंशा थी समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ सकें। इसी के लिए उनका विकेंद्रीकरण, समावेशन और संवाद पर ख़ास ज़ोर था। ये सभी समाज के अंतिम जन को साथ ले कर चलने के लिए रास्ता बनाते थे।
खादी और चरखा स्वावलंबन के साथ साथ रोज़गार और प्रकृति के साथ सह जीवन को भी संभव करते थे। उपभोग की सीमा को पहचानते हुए और भारत की बड़ी जनसंख्या की मुश्किलों के मद्दे नजर वह उपभोग को नियंत्रण में रखने और ज़रूरतों को कम करने पर बल देते थे।
अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी पर स्वतंत्रता पाने के बाद हमारा रुख़ बदलता गया । पश्चिम की छत्र-छाया हर तरफ़ बनी रही। उसे ही श्रेष्ठ मान कर उस पर निर्भरता भी बढ़ती रही। उसे ही आदर्श मानते हुए उसी जैसा बनाते हुए विदेशी का आकर्षण मन में ऐसा बैठा कि मेड इन भारत की मेड इन एनी ह्वेयर को हम पसंद करने लगे। बाजार में विदेश की चीजें और शिक्षा में विदेश की डिग्री को तरजीह मिलने लगी। इस तरह की पसंद से आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी हुईं और अपने में ख़ुद का भरोसा भी डिगने लगा। इन सबसे बढ़ कर पर-निर्भरता एक नए ढंग की पराधीनता को जन्म देने लगी।
आज के वैश्विक माहौल में ऐसा दुराग्रह घातक होता है और उसके दुष्परिणाम भी दूरगामी प्रभाव वाले होते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज द्वारा सतत प्रत्यवलोकन जरूरी हो जाता है ताकि नवीन उभरती परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हुए राह बनाई जा सके। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है । पर मुश्किल यह और बहुत हद तक कल्पनाशील भी । अपनी सीमाओं को सजगता से पहचान कर विकल्पों की खोज करते हुए सारे आविष्कार होते हैं जो भविष्य का निर्माण करते हैं ।
इसके लिए अनुशासन को अपेक्षा होती है । अनुशासन की संस्कृति बाहर से आरोपित नहीं हो सकती उसके लिए अपने को समर्पित कर जीना होगा । स्वदेशी का अभिप्राय अपने देश यानी मातृ भूमि के प्रति हर तरह से अपनत्व की भावना है ।
इस दृष्टि को अपनाते हुए व्यक्ति देश रूपी समष्टि को अपने जीवन और आचरण में स्थान देता है । भारत के स्वातंत्र्य की संघर्ष गाथा में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी का बहिष्कार की केंद्रीय भूमिका रही है । वह मात्र प्रतीकात्मक न हो कर निजी व्यवहार में उतारने का प्रयास था । वर्तमान परिस्थितियों में देश की युवा क्षमताओं को प्रोत्साहित करने और देश की सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए देश को स्वदेशी की ओर आगे बढ़ना होगा।