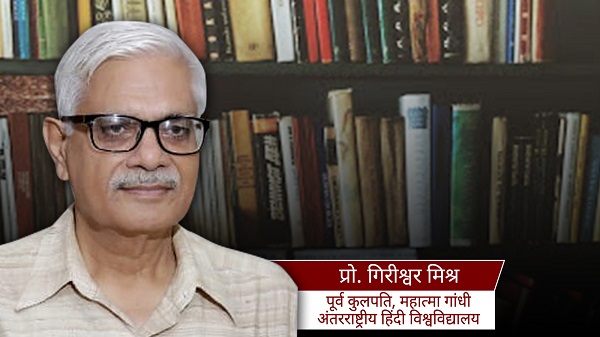Indian knowledge in education: शिक्षा में भारतीय ज्ञान: क्यों और कैसे?
सुनने में यह कुछ अटपटी सी बात लगती है कि भारतीय शिक्षा को अब ‘भारतीय’ ज्ञान-परम्परा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पहल की जा रही है। इसे लेकर आम आदमी के मन में कई सवाल खड़े होते हैं : भारतीय होने का क्या अर्थ है ? जो ज्ञान-परम्परा स्वतंत्र भारत में चलती रही है वह किस अर्थ में भारतीय नहीं थी या कम भारतीय थी ? भारतीय ज्ञान-परम्परा का स्वरूप क्या है ? वह किस रूप में दूसरी ज्ञान-परम्पराओं से अलग है ? इस भारतीय ज्ञान-परम्परा की विशिष्टता क्या है जो हम इसकी ओर मुड़ें ? हालाँकि इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कुछ राजनीतिक पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है पर आज के ज्ञान-युग में सामर्थ्यशाली होने के लिए इस पर विचार करना भारत के लिए किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं कहा जा सकता।
शिक्षा भारत में हो रही है, वह भारतीय शिक्षार्थियों के लिए है और भारतीयों द्वारा ही दी जा रही है। यह लोक-रुचि और लोक-कल्याण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस पर सार्वजनिक विचार होना ही चाहिए । तटस्थता और उपेक्षा का नज़रिया छोड़ कर इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना ज़रूरी है। आख़िरकार यह पूरे समाज की मनोवृत्ति, आचरण और देश के सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल है। शिक्षा की दृष्टि से यह एक गंभीर तथ्य हो जाता है कि हम आलोचनात्मक रूप से चिंतनहीन और सर्जनात्मकता की दृष्टि से पंगु होते जा रहे हैं।
शैक्षिक निष्पादन चिंताजनक रूप से घट रहा है। राजनीति में आडम्बर और मानवीय मूल्य दृष्टि की बढ़ती कमी आज सबको खटक रही है। सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में चिन्ताएँ बढ रही हैं। उदाहरण के लिए न्याय व्यवस्था में आज तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका । आज करोड़ों मुक़दमें हैं जिनमें झूठे मुक़दमे भी हैं और करोड़ों परिवार त्रस्त हैं। नागरिक जीवन से जुड़ी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद नहिं हैं। ऐसे में शिक्षा पर बहुतों की नज़रें टिकी हैं और उसके सुधार से बड़ी आशाएँ जगती हैं।
शिक्षा नीति में भारतीयता की दिशा में बदलाव की पहल के प्रति समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं। पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान को सार्वभौमिक मान रहे लोग इसे राजनैतिक शगूफा मान रहे हैं, कुछ इस मोड़ के प्रति तटस्थ हैं, कुछ थोड़े संभ्रम के साथ उत्सुक हैं। कुछ हैं जो वास्तविक अर्थों में इसे गंभीरता से भी ले रहे हैं पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । जो भी हो भारतीय ज्ञान-परम्परा का नीति-निर्माण की दुनिया में प्रवेश हो चुका है। नई शिक्षा नीति को लेकर देश भर में हुई लगातार हुई चर्चाओं के कई दौर चलने के बाद विभिन्न विषयों के पाठयक्रम भारतीय ज्ञान-परम्परा के प्रति उन्मुख हो रहे हैं और आम जनों के बीच भी इसे लेकर उत्सुकता बढी है। पर शिक्षा में भारतीयता की इस सतही उपस्थिति से आगे बढ कर गम्भीर और व्यवस्थित रूप इस उपक्रम को अभी तक नहीं मिल सका है। कई लोग इसे एक नारा मान कर चल रहे हैं जब कि कुछ के लिए यह अस्मिता और भावना का प्रश्न बन गया है।
यह तो तय है कि यदि पश्चिमी खर्चीले और अंशत: दिशाहीन तथा आयातित ज्ञान को थोपे जाने से मुक्ति की इच्छा है और अपने देश के ज्ञान, कौशल और अस्मिता को बंधक से छुड़ाने का मन है तो शिक्षा में बदलाव लाना ही होगा। यह भी निर्विवाद है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मानसिक स्वराज ज़रूरी है और अपनी ज्ञान-व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। ओढ़ी हुई आधुनिकता की जगह नवोन्मेषी हो कर समकालीन परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी लाना होगा। हमको सांकेतिक और सजावटी बदलाव के भुलावे से आगे बढ़ कर परिस्थितियों का सामना करना होगा और शिक्षा में ज़रूरी रूपांतर भी लाना होगा क्योंकि मानसिक ग़ुलामी कई तरह से देश को आहत करती आ रही है जिसका बहुतों को पता भी नहीं होता। भारत के मानस का वि-उपनिवेशीकरण (डिकोलोनाइज़ेशन) शिक्षा में भारतीय दृष्टि की विवेकपूर्ण संगति के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है। भारत की शिक्षा को भारतीय दृष्टि में स्थापित करने के परिणाम भारत और विश्व दोनों के ही हित में होगा।
ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के पश्चिमी माडेल का खोखलेपन दिन-प्रतिदिन उजागर हो रहा है। अविरल चलती हिंसा, जलवायु-परिवर्तन की बढ़ती मुश्किलें, तीव्र होती गलाकाट प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण का भीषण प्रदूषण, मनुष्यता की जगह बाज़ार का बढ़ता प्रभुत्व और अब कृत्रिम मेधा के क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तनों की सौग़ात ज्ञान के पश्चिमी नेताओं की सोच और मानसिकता पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। यह सारा विकास मनुष्यता के विनाश का कारण बन रहा है।

भारतीय ज्ञान-परम्परा मनुष्य की क्लेशों से मुक्ति की कामना करती है परंतु यह खेद की बात यह है कि बहुतों के मन में इस ज्ञान-परम्परा की वही बेढ़ब और अस्पष्ट छवि अभी भी बरकरार है जो कभी अंग्रेज बहादुरों ने बनाई थी और जिसे क़रीब दो सदियों लम्बे औपनिवेशिक दौर में भारतीयों ने बहुत हद तक आत्मसात् कर लिया था। इसी के चलते आज बहुत से लोग इसे स्वर्णिम अतीत की अनावश्यक स्मृति का ऐसा आग्रह या व्यामोह मानते हैं जो वर्तमान से अछूता है । हालाँकि आज की वैश्विक परिस्थितियों की सच्चाई पश्चिमी ज्ञान को लेकर निराशा ही दिखा रही है और लगातार हो रहे युद्ध से उसके बारे में बचे-खुचे भ्रम टूट बिखर रहे हैं ।
वस्तुतः यह सोच दूषित और दुराग्रहपूर्ण है कि भारतीय ज्ञान-परम्परा के प्रयोजन, परम्परा और दृष्टि संदिग्ध है। सच्ची बात यह है कि भारतीय ज्ञान-परम्परा ज्ञान-विज्ञान भी है और जीवन-दर्शन भी। यह यूरोकेंद्रित सोच-विचार का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करती है और वास्तविक जीवन अनुभव, आचार, नैतिकता और व्यापक सृष्टि की अवधारणाओं से जोड़ती है। भारतीय ज्ञान-परम्परा कोई काल में दफ़्न वस्तु नहीं है। वह जीवित है और विकसित भी होती रही है। हाँ, इसके संस्थागत रूप की निरंतर उपेक्षा होती रही और हम उससे विरक्त होते गए। व्यक्तिवादी, अमूर्त्त, मात्रात्मक, और एकांत अनुशासनों की पक्षधर पश्चिमी ज्ञान परम्परा में सभी विषय स्वतंत्र ढंग से अलग-अलग विकसित हुए हैं
इसकी परिणति अतिरिक्त विशेषज्ञता के विकास में दिख रही है। भारतीय ज्ञान-परंपरा समेकित और अंत:क्रियात्मक है। इस प्रतिमान या पैराडाइम में परस्पर अवलंबन और पूरकता है। न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद और योग आदि में ज्ञान की सुनम्य विधियों, सुचिंतित तर्क और अनुभव का उपयोग करते हैं और इनके बीच आवाजाही भी है । इस परम्परा में मनुष्य को प्रकृति के दोहन-शोषण का एकाधिकार नहीं है क्योंकि मनुष्य को पर्यावरण और ब्रह्मांड में स्थापित है न कि उसका केंद्र है ज्ञान का सामाजिक संदर्भ में स्थित होना और नैतिक मूल्यों पर टिका होना भारतीय ज्ञान परम्परा को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि को पूर्णता तक ले जाता है।
भारतीय ज्ञान-परम्परा के विषय में संदेह और उत्साह की कमी अज्ञानता के कारण है जो सांस्कृतिक विस्मरण के साथ बढ़ता रहा है। शिक्षा नीति–2020 के प्राविधान के बाद भी औपनिवेशिक प्रभाव में पश्चिमी ज्ञान जहां सार्वभौम माना जा रहा है भारतीय ज्ञान स्थानीय मान कर हाशिए पर ही डाला जा रहा है । उसे बेतरतीब ढंग से पश्चिमी ज्ञान के मूल विषय-विस्तार में बैठा दिया जा रहा है चाहे वह संगत हो या असंगत। इस प्रसंग में यह भी भूल ज़ाया जाता हैकि भारतीय ज्ञान परम्पराएँ पुरावशेष न हो कर लोक-जीवन में कई रूपों में सजीव रूप से विद्यमान हैं। पर्यावरण-संरक्षण, नैतिक आचरण, औषधीय उपाय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक ज्ञान की सामग्री आम जनों, जन-जातियों और गावों में इतस्तत: बिखरी पड़ी हैं ।
ज़रूरी दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव में ये विनष्ट हो रही हैं। इस दृष्टि से वाचिक परंपराओं को भी शिक्षा में समाहित करना होगा। जनजातियों, स्त्रियों और विभिन्न समुदायों के ज्ञान प्रायः मुख्य धारा से बहिष्कृत रहते हैं। भारतीय ज्ञान-परंपरा केवल अतीत की ओर नहीं देखती । वह शरीर मन और पर्यावरण के आवश्यक संतुलन पर बल देती है। भारतीय ज्ञान-परंपरा हमारे सभ्यता के उत्कर्ष का साधन बन सकती है बशर्ते हम साहस और विवेक के साथ काम करें। यह परम्परा सब किसी की है और सबके लिए है। भारत की ज्ञान-व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से बहुलता वाली रही है।
इसे पुनर्जीवित करने के लिए लोकतांत्रिक तौर पर समावेशी होना होगा। शास्त्र का आदर आवश्यक है परंतु संस्कार, अभ्यास, आख्यान और जीवन के अनुभव कम महत्व के नहीं हैं। पाठ्यक्रम में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुप्रयोग दोनों की ही जगह होनी चाहिए। भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण के लिए और पश्चिमी ज्ञान के आगे जाने के लिए इनको मुख्यधारा में प्रवेश देना होगा । शिक्षा नीति तो आरंभ है बहु क्षेत्रीय निवेश से ही यह पहल टिकाऊ हो सकेगी। भारतीय ज्ञान-परम्परा पर विचार करते हुए विशाल भारत में संस्कृत के साथ ही तमिल, बौद्ध, जनजातीय और वाचिक परम्पराओं की प्राचीन ऋंखला पर, जो युगों से चलती चली आ रही है, ध्यान देना होगा।
दस्तावेज़ीकरण और प्रचार-प्रसार बहुभाषी और समावेशी होना चाहिए। वस्तुतः एक ऐसे पुनर्जागरण की जो उपनिवेश से मुक्ति दिला सके, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी । इसे एक बौद्धिक अवसर के रूप में देखा जना चाहिए। ऐसे समृद्ध पाठ्यक्रम जो अंतरानुशासनिक नज़रिए को आगे बढ़ाएँ ज़रूरी होंगे । तभी भारतीय ज्ञान-परम्परा को समाज विज्ञान, मानविकी, और जीवन विज्ञान, तकनीकी आदि के विषयों के साथ जोड़ा जा सकेगा। पाठ्यक्रम में बिना गंभीर सुधार लाए कोई सार्थक सामाजिक -आर्थिक परिवर्तन नहीं आ सकेगा। इसके लिए सार्वजनिक और निजी निवेश के साथ गंभीर अकादमिक पहल ज़रूरी है।
देश की आवाज की खबरें फेसबुक पर पाने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें