International Yoga Day: योग: कर्मसु कौशलम् !
International Yoga Day: शब्द बड़े चमत्कारी और शक्तिशाली उपकरण होते हैं। शायद इसी को ध्यान में रख कर भारत में वैदिक युग से ही वाक्शक्ति की लगातार अभ्यर्थना की जाती रही है और अक्षर ब्रह्म की परिकल्पना भी की गई । वाक्शक्ति को देवी का दर्जा दिया गया। शब्दों के सराहे हम जीवन में अपने सारे काम करते हैं, कल्पना भी करते हैं, प्रेरित होते हैं, लक्ष्य की योजना बनाते हैं और सृजन में भी प्रवृत्त होते हैं। इसका ताज़ा प्रमाण वर्तमान काल में ‘योग’ शब्द के प्रयोग में दिख रहा है। आज योग एक बड़ा ही लोकप्रिय और लुभावना शब्द हो गया है जिसका धड़ल्ले से सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है ।
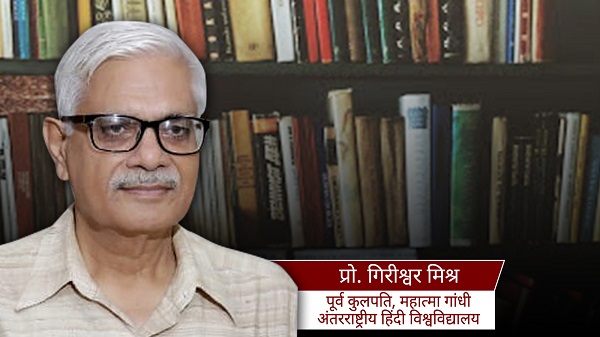
शाब्दिक अर्थ को लें तो योग यानी जोड़, जोड़ने की प्रक्रिया और जोड़ने के परिणाम दोनों को ही व्यंजित करता है। ध्यान से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि योग एक बड़ी ही सर्जनात्मक अवधारणा की ओर ध्यान दिलाता है। आप जैसे हैं वैसे ही निर्विकार या निश्चेष्ट बने रहें या कहें कि आपमें कोई योग अथवा कोई जोड़ न हो, कोई बदलाव या अभिवृद्धि न हो तो ज्ञान या कर्म किसी स्तर पर विकास या प्रगति की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं बनेगी । यह तो मृत होने की स्थिति है। इसीलिए उपनिषद में ऋषि ने प्रार्थना की – मृत्योर्मामृतं गमय । अर्थात् मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो।
आम फ़हम भाषा में योग का एक दूसरा अर्थ अवसर भी होता है। इसी आशय से बातचीत में अक़्सर कहा जाता है कि इसका योग (मुहूर्त!) नहीं बन रहा है या योग ही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर यह कहना ज़रूरी है कि अवसर स्वतः अपने आप घटित होने वाला कोई आकस्मिक संयोग या चमत्कार नहीं होता बल्कि उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए उद्योग करना करना ज़रूरी है । योग बना तो उसे सुयोग में बदलने के लिए आदमी को मेहनत मशक़्क़त करनी पड़ती है। तभी वह फलदायी होता है और हमें मनोवांछित सुख देता है।
इसीलिए कहा गया कि उद्योगी मनुष्य ही लक्ष्मी या धन-सम्पदा को प्राप्त करता है – उदयोगिन: पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी । उस उद्योगी के पास ही श्री का भी आगमन होता है। जो श्रम करने से कभी थकता और कतराता नहीं, उसी के पास धन सम्पदा आती है – नानाश्रांताय श्रीरस्ति । जीवन का मधु निरंतर सक्रिय बने रहने में ही है इसलिए निर्देश दिया गया कि सदैव श्रम करते रहो – चरेवैति चरेवैति चरन् वै मधु विंदति । भगवान कृष्ण योगके महान प्रवक्ता अर्थात् योगीश्वर और कर्मठ जीवन के साक्षात् विग्रह हैं। उनकी लोकविख्यात कथा जीवन में अविराम निरंतर उत्कर्ष का प्रमाण है। प्रभु श्रीराम भी हमारे सम्मुख कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा ही दिखाते हैं। आधुनिक काल में भी जो महान व्यक्ति हुए हैं और आज भी जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं वे सभी श्रम की ही प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। वे सच्चे अर्थों में योगी हैं ।
दुर्भाग्य सेआज कलयोग शब्द का प्रयोग एक बिकाऊ वस्तु के रूप में रूढ़ होता जा रहा है। अनेक लोग इस शब्द का उपयोग शारीरिक आसनों और प्राणायाम अर्थात् साँसों को नियमित करने के तरीक़ों को बताने के लिए किया जाता है। लोग यह कहते सुने जाते हैं कि हम योग या योगा करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए योग की ओर झुकाव स्वास्थ्य और सौंदर्य की कमियों को दूर करने की ओर रहता है। आकर्षक रूप रंग सबको प्रिय होता है और आज सौंदर्य प्रसाधनों का बाज़ार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह सब इंगित करता है कि शरीर-सौष्ठव के प्रति रुझान आज के दौर में एक बड़ा सरोकार बन गया है ।
योग का यह भी एक अर्थ है पर निश्चय ही बड़ा सीमित अर्थ है । श्रीमदभगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म में कुशलता यानी दक्षता प्राप्त करने के रूप योग की अवधारणा को समझाया है। उनके शब्द हैं : योग: कर्मसु कौशलं । इस अर्थ में योग अपने कार्य को उत्कृष्ट बनाने की कला है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि के आठ अंग शरीर, मन और आत्मा को साधने की प्रक्रिया के ही अवयव हैं। कार्य में उत्कृष्टता कितनी उपयोगी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म में उत्कृष्टता है तो मनुष्य यश और कीर्ति का भागी होता है तो इसमें चूक के भयंकर और दुखदायी परिणाम होते हैं।
अपने कार्य में उत्कृष्टता के लिए कार्य के प्रति समर्पण, संलग्नता और आवश्यक हुनर का व्यावहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इन सबके लिए धैर्य और सतत संलग्नता ज़रूरी होती है। चिंता की बात यह है कि ये विचार अब अल्पकालिक या दीर्घकालिक जीवन लक्ष्य के रूप में ज़्यादातर लोगों के लिए आकर्षक नहीं रहे । आज की विडम्बना यह है कि तेज रफ़्तार से बदलते इस दौर में लोग शांति, स्थिरता, धैर्य, समत्व और संतुलन जैसे विचार केवल पिछड़ेपन और कमजोर इच्छाशक्ति के लक्षण मानने लगे हैं ।
लोगों को लगता है कि दौड़-धूप भरी जिंदगी इनके भरोसे नहीं चल पाएगी । गति की तीव्रता का आकर्षण आज के युवा वर्ग में ख़ास तौर पर बढ़ रहा है। साथ ही आत्म-प्रकाशन की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। लोग अपनी छवि बनाने और भुनाने में मशगूल हैं और खुद से दूर होते जा रहे हैं । उनको अपने आपको समझने और गुण दोषों को समझने के लिए उनके पास अवकाश नहीं है। अब असरदार स्टंट करना, आकर्षक रील बनाना और कुछ सनसनीख़ेज़ कारनामे देख या दिखा कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर छा जाना उन्हें बड़ा रास आता है। लाइक बटोरना और सब्सक्राइब होना उनका प्रिय शग़ल बनता जा रहा है और प्रतिदिन अच्छा खा समय उस पर ज़ाया जाता है।

गति, उत्तेजना और क्रियाशीलता को लगातार बढ़ते हुए अनुभव करते रहना लोगों का पसंदीदा व्यसन हो रहा है और उससे ही अधिकाधिक सुख पाने की चेष्टा की जाती है । विडियो गेम तो निष्क्रिय स्थिति में भी सक्रियता का तीव्र आभासी (नकली) अनुभव दिलाते हैं । पर इन सब से जल्दी ही ऊब होने लगती है और किसी नए तरीक़े या उपकरण की तलब होती है । उत्तेजना को बनाए रखने के लिए गेम में विविधता लाई जाती है। इस प्रवृत्ति का सबसे बुरा असर हमारे ध्यान की क्षमता और आदत पर पड़ रहा है । ध्यानावस्थित होने की बात तो दूर किसी बात या वस्तु पर ध्यान देने की हमारी क्षमता ही तेज़ी से घटती जा रही है और उसी के साथ स्मरण शक्ति भी घट रही है । और तो और किसी चित्र पर हमारी आँख सिर्फ़ कुछ पल के लिए ही टिक पाती है। बिना ध्यान दिए वस्तुएँ पकड़ में नहीं आतीं और मानस पटल पर अंकित नहीं होतीं और न हमें उनकी धारणा ही होती है । फलतः वे बहुत जल्द भूल जाती हैं।
धारणा और ध्यान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।हमारी डिजिटल दुनिया का जलवा यही है कि वह ध्यान की क्षमता की बलि ले रही है। दूसरी ओर बाज़ार में वस्तुओं का बढ़ता जमघट हममें अभाव और दीनता का भाव भर रहा है। इसके चलते हमारा अहं भाव और शेष प्रकृति से अलगाव और वैशिष्ट्य का बोध प्रबलतर होता जा रहा है। हम अपने को प्रकृति के अंग के रूप में न देख कर उसके स्वामी के रूप में देखने लगे हैं। इस आत्मविश्वास और संभ्रम की स्थिति को यदा कदा भू स्खलन और बेमौसम वर्षा, सूखा और बाढ़ आदि की घटनाओं से ज़रूर धक्का लगता है।
जीवित सृष्टि और दृश्यमान जगत में जो भी विद्यमान है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पाँच महाभूतों या तत्वों से ही बना हुआ है। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि हमारे शरीर के स्तर पर यही सारे तत्व हमारा भी निर्माण करते हैं जैसा कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी की प्रसिद्ध उक्ति – क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम सरीरा – में ध्वनित होता है । इन पाँच भूतों का अस्तित्व और महत्व सामान्यतया हमारे ध्यान में नहीं आता ।
इन्हें धरोहर न मानकर ख़ैरात में मिली अपनी सम्पत्ति मानते हैं और इनकी अवहेलना और दुरूपयोग करने से बाज नहीं आते ।आज हमारा पर्यावरण ख़तरे में हैं । जल , वायु और पृथ्वी सभी घनघोर प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। इनमे से वातावरण प्रदूषित और क्षुब्ध हो चला है । श्वांस प्रश्वास तो प्राण का आधार है वह भी प्रभावित हुआ । इनसे परे स्वयं को सारी सृष्टि का केंद्र मान बैठना और उसी केंद्र को परम सत्य मन कर आचरण और व्यवहार हमारा अभ्यास बनाता गया है ।
हमने पर्यावरण के बीच का आधारभूत साम्य भुला दिया है। अहंकारदीप्त मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मान बैठा और खुद को उपभोक्ता और पर्यावरण को उपभोग्य बना दिया।
आज तटस्थ भाव से आत्मावलोकन और आत्मपरीक्षा जीवन की एक बड़ी आवश्यकता हो चली है। इसी से मानवीय विवेक का उदय होगा। इसके लिए योग की सहायता से हम अपनी स्वयं अपनी अंतर्यात्रा करते हैं । यानी अपने भीतर झांकते हुए शरीर, मन और आत्मा के साथ संवाद करते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हुए आत्मोन्नयन के लिए उद्यत होते हैं। जीवन के विस्तृत प्रांगण में आनंद और सौंदर्य अपने सीमित स्व से परे जा कर ही मिलता है। योग इसी का प्रशस्त यात्रापथ है जिसका उद्देश्य अपने स्वरूप को पहचान कर अपने नियत कर्तव्य पर आगे बढ़ना है। कर्म में कुशलता ले आने का प्रयोजन अपना तथा अपने देश और समाज का अभ्युदय करना है।
देश की आवाज की खबरें फेसबुक पर पाने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें
